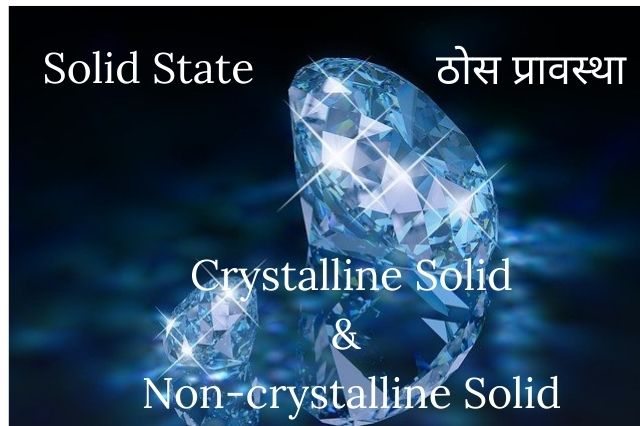Contents [show]
ठोस (Solid)-
वे पदार्थ जिनमें असंपीड्यता, दृढ़ता और यांत्रिक सामर्थ्य होती है उन्हें ठोस पदार्थ कहा जाता है ।
Meanings
असंपीड्यता – Incompressibility
दृढ़ता – Rigidity
यांत्रिक सामर्थ्य- Mechanical Strength
ससंजक बल – Cohesive Force
ठोसों के प्रकार (Type Of Solids)
क्रिस्टलीय ठोस –
वे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई एक नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं ।
उदाहरण – हीरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयोडीन ।
रचक इकाई – आयन या परमाणु या अणु होते हैं ।
क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण –
- अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं ।
- ये तीक्ष्ण एवं निश्चित गलनांक रखते हैं ।
- क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है ।
- ये विषमदैशिक होते हैं ।
विषमदैशिक – ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो विषमदैशिक होते हैं इनके भौतिक गुण
जैसे- विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता, अपवर्तनांक, विस्कासिता, यांत्रिक जड़ता आदि विभिन्न दिशाओं में भिन्न–भिन्न होते हैं ।
द्विअपवर्तन- यदि किसी क्रिस्टल में से कोई प्रकाश की किरण प्रवाहित होती है । तो वह किरण विभिन्न घटकों में विभक्त हो जाती है । प्रत्येक घटक विभिन्न पथ से और विभिन्न वेग से चलता है । इस घटना को द्विअपवर्तन कहते हैं ।
Meanings –
क्रिस्टलीय ठोस- Crystalline Solids
आयन – Ion
परमाणु- Atom
अणु – Molecule
रचक इकाई – Constituent Unit
नियमित – Regular
क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण – Characteristics of Crystalline Solids
तीक्ष्ण या निश्चित – Sharp
विषमदैशिक – Anisotropic
द्विअपवर्तन – Double Refraction
अक्रिस्टलीय ठोस – Non- Crystalline or Amorphous Solid
बहु क्रिस्टलीय ठोस – Polycrystalline Solid
अक्रिस्टलीय ठोस (Non- Crystalline or Amorphous Solid )
वे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं रहती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं ।
जैसे – कांच, प्लास्टिक, रबर आदि ।
अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण –
समदैशिक –
- अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं ।
- ये तीक्ष्ण एवं निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं ।
- ठोस निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम नहीं दर्शाती है ।
- ये समदैशिक होते हैं ।
- ये आभासी ठोस होते हैं ।
- वास्तव में ये आभासी ठोस होते हैं वास्तव में ये अतिशितीत द्रव होते हैं ।
- ये ठोस कटी सतह पर भी रचक घटकों का अनियमित क्रम रखते हैं अर्थात् इनका विदलन नहीं होता है ।
- ये गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं ।
- अक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने वाला श्रेष्ठतम उपलब्ध प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है ।
- इसमें कुछ सीमा तक समपीड्यता तथा दृढ़ता पायी जाती है ।
- इनमें स्थितीज ऊर्जा का मान, क्रिस्टलीय पदार्थों की अपेक्षा अधिक होता है ।
अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं । इसका कारण यह है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में अणु, परमाणु या आयन अनियमित तथा अव्यवस्थित होते रहते हैं । अत: सभी दिशायें समान रहती हैं और विभिन्न दिशाओं में सभी गुण समान होते हैं ।
Meanings –
समदैशिक – Isotropic
अति प्रशीतित द्रव – Supercooled Liquids
संपीड्यता – Compressibility
गलनांक – Melting Point
बहुक्रिस्टलीय ठोस –
कुछ ठोस पदार्थ पाउडर के रूप में या संपीडित कणों के रूप में होते हैं । और ये अक्रिस्टलीय महसूस होते हैं । जबकि इसकी एक निश्चित क्रिस्टलीय आकृति होती है इस बात का पता माइक्रोस्कॉप में प्रत्येक कण को देखने से पता चलता है ।
या
वे ठोस जिनमें क्रिस्टल इतने छोटे होते हैं कि वे केवल उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कॉप द्वारा ही देखे जा सकते हैं । सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस अथवा बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं ।
Meaning –
बहुक्रिस्टलीय ठोस – Polycrystalline Solids
संपीडित – Agglomerate
सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस – Microcrystalline Solids
क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण (Classifications of Crystalline )
विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है ।
1 आयनिक ठोस या क्रिस्टल
2 आण्विक ठोस या क्रिस्टल
3 सह-संयोजी ठोस या क्रिस्टल
4 धात्विक ठोस या क्रिस्टल
आयनिक ठोस/ क्रिस्टल –
वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचना धनायन व ऋणायन से मिलकर बनती है, आयनिक क्रिस्टल/ठोस कहलाते हैं ।
उदाहरण – NaCl, CsCl, ZnCl2, KNO3
आयनिक ठोसों के लक्षण –
1 ये धन व ऋण आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं जैसे Na+ व Cl– आयन NaCl में संरचनात्मक इकाई होती है ।
2 ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं ।
3 ये ठोस कठोर व भंगुर प्रवृत्ति रखते हैं ।
4 ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखने के कारण अवाष्पशील होते हैं ।
5 ये ठोस प्रबल विद्युत आकर्षण बल रखते हैं । इसी कारण ये उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक भी रखते हैं ।
6 विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलॉम का आकर्षण बल होता है ।
7 ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं ।
8 ठोस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते हैं जबकि गैस व द्रव अवस्था में आयन गतिशील होते हैं ।
Meanings –
आयनिक ठोस – Ionic Solid
कूलॉम – Coulomb
कठोर – Hard
भंगुर – Brittle
प्रबल – Strong
उच्च – High
वाष्पन ऊष्मा – Heat Of Vaporisation
अवाष्पशील – Non-Volatile
ध्रुवीय विलायको – Polar Solvents
विद्युत के कुचालक – Bad Conductor
गलित – Fused
आण्विक/अणुक ठोस / क्रिस्टल
ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचना इकाई अणु होती है आण्विक ठोस/क्रिस्टल कहलाते हैं ।
जैसे – I2 , CH4 (s), शुष्क बर्फ, CO2 (s),
यहां s का मतलब ठोस (Solid) होना है ।
इनके क्रिस्टल में अणुओं के मध्य वाण्डर वाल्स बल पाया जाता है ।
ध्रुवीय आण्विक ठोस जैसे ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) द्विध्रुव-द्विध्रुव बंधन बल रखते हैं ।
अध्रुवीय आण्विक ठोस जैसे ठोस ऑक्सीजन (O2) लण्डन बंधन बल रखते हैं ।
कुछ आण्विक ठोस हाइड्रोजन बंधन बल भी रखते हैं, जैसे – ठोस अमोनिया (NH3), बर्फ (H2O)
आण्विक ठोसों के लक्षण –
1 ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं ।
2 इनमें अंतरकण, बंधन बल, वाण्डर वॉल्स बल होता है ।
3 ये ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं ।
4 ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायको में विलेय होते हैं ।
5 ये निम्न वाष्पन ऊष्मा रखने की वजह से सामान्यत: वाष्पशील होते हैं ।
6 ये ठोस मुलायम होते हैं ।
7 इनके मध्य दुर्बल वाण्डर वॉल्स बल होने के कारण ये निम्न गलनांक व निम्न क्वथनांक रखते हैं ।
Meanings –
अणुक क्रिस्टल – Molecular Crystals
वाण्डर वॉल्स – Vander Waals
निम्न – Low
सहसंयोजी ठोस/ क्रिस्टल –
ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है, सहसंयोजी ठोस/ क्रिस्टल होते हैं ।
उदाहरण – हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, सिलिकॉन, कार्बाइड । इनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाये जाते हैं । इन बंधो के द्वारा इस प्रकार के ठोस विशाल अंतरबंधीय संरचना रखते हैं । इसलिये इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं ।
लक्षण –
1 ये ठोस परमाणुओं द्वारा बने होते हैं ।
2 इन ठोसों में सहसंयोजक अंतरकण बंधन होता है ।
3 ये ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं ।
4 ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखते हैं जिसके कारण अवाष्पशील भी होते हैं ।
5 ये अतिकठोर व भंगुर होते हैं ।
6 नेटवर्क ठोस होने के कारण ये अत्यधिक उच्च गलनांक व क्वथनांक भी रखते हैं ।
7 सहसंयोजी ठोसों में ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है ।
8 प्राकृतिक पदार्थों में हीरा सर्वाधिक कठोर होता है ।
9 ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षट्भुजीय इकाई युक्त परते बनाते हैं ।
10 प्रत्येक कार्बन परमाणु अपनी परत के तीन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है ।
11 प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन दो परतों के मध्य मुक्त अवस्था में रहता है ।
12 मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक व परतों की एक दूसरे पर सरक सकने के कारण मुलायम एवं ठोस स्नेहक जैसा होता है ।
13 सहसंयोजी ठोसों में धात्विक चमक होती है ।
Meanings –
गलनांक – Melting Point
सहसंयोजक ठोस – Covalent Solid
धात्विक ठोस/क्रिस्टल –
वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होती है, धात्विक ठोस कहलाते हैं । जैसे कॉपर, रजत, निकल
लक्षण –
1 इनके परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाये जाते हैं ।
2 ये ठोस धातु परमाणुओं द्वारा बने होते हैं ।
3 ये निम्न से उच्च वाष्पन रखते हैं ।
4 ये तन्य व आघातवर्धनीय होते हैं ।
5 ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं ।
6 ये निम्न से उच्च गलनांक व क्वथनांक भी रखते हैं ।
7 ये अतिमुलायम से अतिकठोर होते हैं । जैसे – सोडियम अति मुलायम व ऑसमियम अति कठोर है ।
8 इनमें परमाणु जब संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब परमाणु का शेष भाग धनावेशित हो जाता है । इस प्रकार धनावेशित भाग व इलेक्ट्रॉनो के मध्य आकर्षण बल धात्विक बंध बनता है ।
Meanings –
तन्य – Ductile
आघातवर्धनीय – Malleable
धातु परमाणु – Metal Atoms